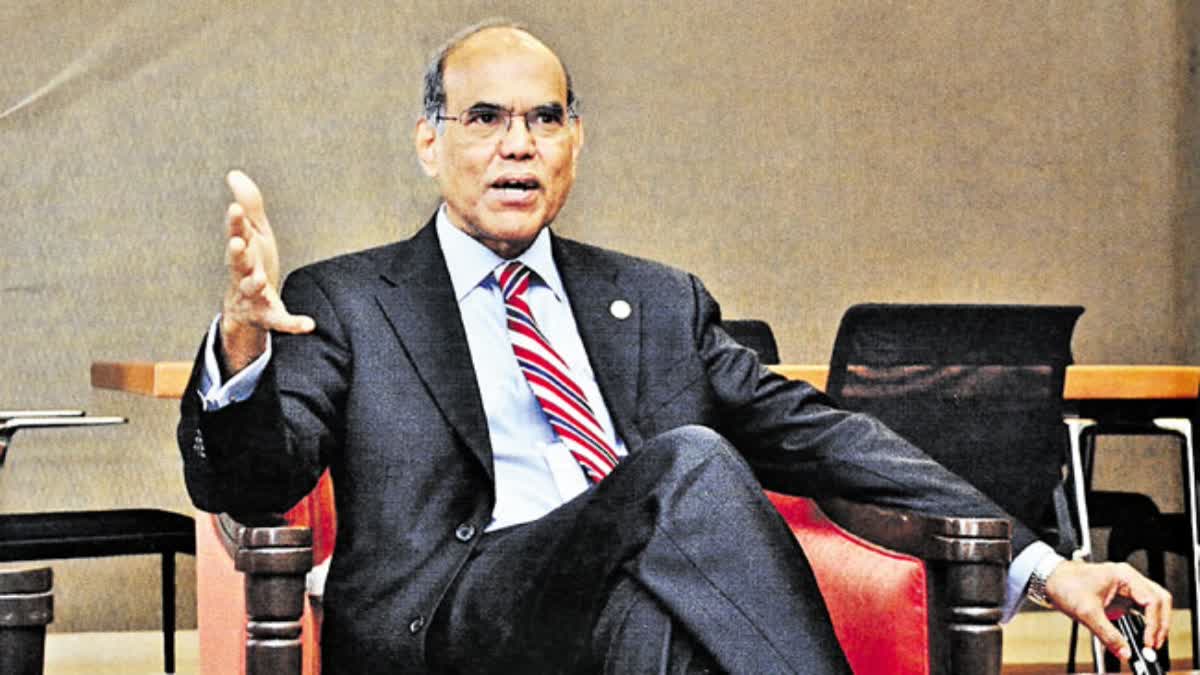हैदराबाद: यद्यपि राज्य और केंद्र तत्काल सहायता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और नकद हस्तांतरण योजनाएं लागू कर रहे हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य और शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन पर कोई फोकस नहीं है. गरीब लोगों को गरीबी की प्रकृति पर विचार करना चाहिए और अल्पकालिक और दीर्घकालिक पहलुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए.
रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव का मानना था कि अगर आज बहुत हुआ तो उन्हें कभी भी पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा. उनका कहना है कि इन 50 वर्षों में सिविल सेवा में कई बदलाव हुए हैं, हर तरह की पृष्ठभूमि से लोग आ रहे हैं और महिलाओं की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा कि आईआईटी और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से अधिक लोगों का सिविल सेवा में आना एक अच्छा विकास है.
गोदावरी के तट पर कोव्वुरु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए दुव्वुरी सुब्बाराव को आईएएस के लिए चुना गया था और उन्होंने केंद्रीय वित्त विभाग के सचिव, विश्व बैंक में अर्थशास्त्री तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया. उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के साथ 'जस्ट ए मर्सिनरी?' शीर्षक से एक किताब लिखी है.
इसमें उन्होंने आईआईटी कानपुर के छात्र के रूप में सिविल सेवाओं के लिए चयनित होने, अपना प्रशिक्षण पूरा करने और पार्वतीपुरम में उप-कलेक्टर के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग पाने से लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक के अपने अनुभवों के बारे में बताया है. इसे लेकर उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़ें इस बातचीत के कुछ खास अंश...
प्रश्न: आपके सेवा में आने के बाद से भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या बदलाव हुए हैं?
उत्तर: मुझे आईएएस में शामिल हुए लगभग पचास साल हो गए हैं. इन पचास सालों में बहुत कुछ बदल गया है. भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर प्रबंधन, विशेषज्ञता, आदि. सेवा में आने वाले अधिकारियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि बदल गई है. जब हम शामिल हुए, तो 20 से 25 प्रतिशत पहले से ही सेवा में मौजूद लोगों के बच्चे थे. अब सभी पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं.
दूसरा, तब महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और हाल के दिनों में काफी बढ़ी है. परीक्षा पैटर्न समेत कई पहलुओं में बदलाव हुए हैं. जब हम प्रशिक्षण से बाहर आए तो गरीबी उन्मूलन मुख्य फोकस था. अब स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ज्यादा फोकस है. जवाबदेही बढ़ी है. तब ऐसा नहीं था.
तब उन्होंने सोचा कि चाहे हम पानी, बिजली और सड़क जैसी चीजों के लिए कुछ भी कर लें, हम जीवित रहेंग. अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मांग की स्थिति बढ़ गयी है. उप-कलेक्टर और कलेक्टर के रूप में काम करते समय, जब उन्होंने स्थानीय सरपंच, समिति अध्यक्ष, विधायक और सांसद से चर्चा की, तो वे सिविल सेवा अधिकारियों की तुलना में कम शिक्षित थे.
एक राय थी कि सिविल सेवा अधिकारी उनसे श्रेष्ठ थे. अब स्थिति अलग है. कुछ स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पीएचडी की है. अब तो जन प्रतिनिधि भी सोचते हैं कि हम बराबर हैं. प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई है. लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलीं. समर्पण, ईमानदारी और व्यावसायिकता तब और अब भी वही हैं. एक सिविल सेवा अधिकारी के लिए जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए.
पूर्व आरबीआई गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव का कहना है कि 'हम सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हम कहते हैं कि विकास दर 7 फीसदी है. एक सवाल यह है कि अगर विकास इतना तेज़ है तो बेरोज़गारी क्यों है? उसके कई कारण हो सकते हैं. रोजगार के अवसर पैदा करने वाला विकास आवश्यक है. सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए.'
प्रश्न: हमारे देश को दीर्घकालिक विकास के लिए किन रणनीतियों और नीतियों का पालन करना चाहिए? हमारे सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
उत्तर: आर्थिक चुनौतियों में एक विशेष रूप से बड़ी समस्या नौकरियां हैं. हम सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हम कहते हैं कि विकास दर 7 फीसदी है. एक सवाल यह है कि अगर विकास इतना तेज़ है तो बेरोज़गारी क्यों है? उसके कई कारण हो सकते हैं. रोजगार के अवसर पैदा करने वाला विकास आवश्यक है.
उस पर ध्यान दें. विकास तो बढ़ रहा है, लेकिन लाभ सभी को नहीं मिल रहा है. असमानताएं बढ़ रही हैं... कम होनी चाहिए. आइए देखें कि निम्न स्तर पर आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं. अमेरिका आगे है क्योंकि वह एक नवोन्वेषी समाज है. फेसबुक, अमेज़न और गूगल जैसी बेहतरीन कंपनियां हैं. ऐसे नवोन्मेषी समाज के निर्माण के लिए अनुसंधान और उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्र से आकर आरबीआई के गवर्नर जैसे उच्च पद तक पहुंचना कैसे संभव है? इस क्रम में आपके लिए कौन सी चीज़ें एक साथ आई हैं?
उत्तर: कहना जरूरी है कि यह देश महान और गौरवान्वित है. ये बात मेरी किताब में भी लिखी है. समाज ने मुझे यह अवसर दिया. मेरा जन्म एक ग्रामीण इलाके में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और सिस्टम द्वारा दिए गए अवसरों के कारण मैं इस तरह बड़ा हुआ. मैंने सैनिक स्कूल में छात्रवृत्ति से पढ़ाई की. मेरे पिता के पास छात्रवृत्ति के बिना मुझे वहां भेजने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे.
मैंने आईआईटी में भी स्कॉलरशिप से पढ़ाई की. बाद में आईएएस में भी. योग्यता के आधार पर, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड और सेवा में अनुभव के आधार पर, मुझे रिज़र्व बैंक का गवर्नर बनने की अनुमति दी गई. हमने जो पढ़ा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने उसे कितनी अच्छी तरह पचाया है और हम कितने परिपक्व हुए हैं. इस देश और इस समाज ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ दिया है.
प्रश्न: आप इस राय को कैसे देखते हैं कि देश आईएएस अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है?
उत्तर: यह कहना थोड़ी अतिशयोक्ति है कि देश आईएएस अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है. एक बार यह सच था... अब तो कई नेता भी पढ़े-लिखे लोग हैं. आईएएस अधिकारियों को नीतिगत मुद्दों पर राजनेताओं को अपने फायदे और नुकसान बताने चाहिए. इसके अनुसार राजनीतिक मशीनरी निर्णय लेती है.
प्रश्न: राज्य शासन और केंद्रीय शासन के बीच क्या अंतर हैं? उनसे क्या सीखा जा सकता है और क्या छोड़ा जा सकता है?
उत्तर: वास्तव में कुछ अंतर हैं. राज्य का प्रशासन सीएम द्वारा चलाया जाता है. सीएम जो कहेंगे वही होगा. लेकिन केंद्र में कुछ प्रणालियां हैं. प्रधानमंत्री जो भी सोचेंगे, कैबिनेट कमेटी और सचिवों की व्यवस्था उसमें अच्छे-बुरे की जांच करेगी. वह व्यवस्था राज्य में नहीं है. यानी अगर मुख्यमंत्री कहीं जाकर 30 करोड़ रुपये लगाकर अस्पताल बनाने का वादा करेंगे तो वे सोचेंगे कि पैसा कहां से आयेगा.
केंद्र में ऐसा कम ही होता है. राज्य में अधिकारियों और राजनेताओं का दायरा सीमित है. केंद्र में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारी हैं. उनसे सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है. यदि आप राज्य में काम करते हुए केंद्र में जाते हैं, तो आप विभिन्न राज्यों के अधिकारियों से नई चीजें सीख सकते हैं और राज्य वापस आने पर उन्हें लागू कर सकते हैं.
किसी राज्य में नौकरी करके अखिल भारतीय सेवा करना उचित नहीं है. केंद्रीय और राज्य सेवाओं में काम करना महत्वपूर्ण है. दो साल से भी कम समय पहले, जब यह प्रावधान किया गया था कि आईएएस को केंद्रीय सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहिए, तो राज्यों ने आपत्ति जताई थी. राजनीति के कारण इसे लागू नहीं किया गया.
प्रश्न: हाल ही में आईआईटी से सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण है? इसके कारण सेवा में क्या परिवर्तन आये?
उत्तर: किसी भी व्यक्ति के लिए आईएएस परीक्षा पास करने के लिए एक डिग्री ही काफी है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा विषय पढ़ते हैं. आईएएस का मतलब पढ़े गए विषय में नौकरी पाना नहीं है... आपको सभी पहलुओं की व्यापक और गहरी समझ की आवश्यकता है. मैंने इसे पढ़ा क्योंकि मुझे भौतिकी में रुचि है.
सेवा में शामिल होने के चार साल बाद, मैंने सोचा कि और पढ़ना अच्छा रहेगा. सबसे पहले अर्थशास्त्र का अध्ययन करना लाभदायक है. सबसे पहले मैं इंजीनियर बनने की इच्छा से आईआईटी में शामिल हुआ. तब एक राय थी कि आईएएस का मतलब राजनीति विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करने वालों के लिए है. लेकिन आईआईटी में प्रतिभा आती है.
देश में पढ़ाई में अव्वल रहने वाले लोग वहां जाते हैं. आईआईटी में पढ़ने वाले सिर्फ इंजीनियर ही नहीं होते, वो अच्छा लिख भी सकते हैं और बॉलीवुड में एक्टिंग भी कर सकते हैं. देश की सेवा के लिए हर तरह की प्रतिभा की जरूरत होती है. आईआईटी से सेवा में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि एक अच्छा विकास है.
प्रश्न: आपके समय में आईएएस अधिकारियों को नियमों के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिला था. क्या अब ऐसी आज़ादी और स्वच्छंदता है? कहा जाता है कि नेताओं का दबदबा बढ़ गया है और वे जो कहते हैं अगर वो नहीं करते तो आईएएस के लिए भी हालात मुश्किल हो गए हैं. क्या यह मूल्यों में गिरावट का संकेत है? आप क्या कहते हैं?
उत्तर: मुझे आरबीआई छोड़े हुए दस साल हो गए हैं. आईएएस छोड़ने के 15 साल हो गए. तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है. सिविल सेवा अधिकारियों और राजनेताओं के बीच अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है. क्योंकि राजनेता राजनीतिक रूप से गलत हैं. सिविल सेवा अधिकारियों को नियमों के मुताबिक काम करना होगा. इसलिए कुछ मामलों में असहमति और मतभेद अपरिहार्य हैं.
सिविल सेवा अधिकारियों को निष्पक्ष सलाह और सुझाव देना चाहिए. यही सिविल सेवा का मूल सिद्धांत है. राजनीतिक लाभ के लिए दबाव डाला जाता है, लेकिन सिविल सेवा अधिकारियों को यह सीखने की जरूरत है कि प्रबंधन कैसे किया जाए. हर बात को नकारना गलत है. जनहित में जो किया जा सकता है उसे करना और जो नहीं किया जा सकता उससे इंकार करना.
यह तौलना जरूरी है कि हम जो फैसला लेते हैं, वह जनहित में है या खिलाफ. उदाहरण के लिए, कलेक्टर ने एक टीकाकरण योजना तैयार की है... एक विधायक आता है और कहता है कि इसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक लोगों को दें... क्या हमें उस पर आपत्ति है? समायोजित करना? क्योंकि विधायक ने जो पूछा वह भी जनता के लिए है.
प्रश्न: सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान फील्ड स्तर पर जाने में क्या अंतर है?
उत्तर: उस समय सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी. अब सेल फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गए हैं. उस वक्त हम फील्ड लेवल पर जाते तो हमें कुछ पता नहीं चलता था. अब बिना जाए ही किसी भी जगह से देखा जा सकता है. इसके अलावा, यदि सिविल सेवक फील्ड स्तर पर नहीं जाते हैं, तो वे कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते हैं. सीधे जाकर लोगों से बात करके आप नए अनुभव हासिल कर सकते हैं. फ़ील्ड यात्राएं प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं.
प्रश्न: केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर पहले से ही मतभेद और विवाद हैं. इसका सही समाधान क्या है?
उत्तर: ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि हर देश में राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद होते हैं. यदि करों का हिस्सा हस्तांतरित किया जाए और निवेश निष्पक्ष रूप से किया जाए तो यह देश के लिए अच्छा है. पूरा देश आगे बढ़े तो अच्छा होगा. किसी भी राज्य की खुद को विकसित करने की इच्छा समझ में आती है. यदि राज्य विकास में प्रतिस्पर्धा करें तो यह देश के लिए अच्छा है.
केंद्र सरकार माता-पिता के समान है. इसलिए निष्पक्ष होकर कार्य करें. यह देखना चाहिए कि लोगों को यह लगे कि हम वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी धारणा न बने कि एक राज्य या क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, अधिक पैसा दिया जा रहा है, निवेश और बुनियादी ढांचा वहां जा रहा है और निजी निवेश वहां भेजा जा रहा है. यह देश और राज्यों के लिए अच्छा है.
प्रश्न: आपने संयुक्त एपी, केंद्र, आईएमएफ, विश्व बैंक, आरबीआई आदि में काम किया है. आपको सबसे अधिक चुनौतियों का सामना कहां करना पड़ा है?
उत्तर: मैंने साढ़े तीन दशकों तक एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम किया. इसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और 6 साल तक विश्व बैंक में काम किया. अपने करियर के अंत में मैंने रिज़र्व बैंक में काम किया. हर काम की अपनी चुनौतियां होती हैं... अपना आकर्षण होता है. सिविल सेवा का सबसे बड़ा आकर्षण कार्यों और अनुभवों की विविधता है.
यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी से जुड़ते हैं, तो उसमें आपकी उन्नति होगी. करियर का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र से शुरुआत करता है. आईएएस के लिए ऐसा नहीं है... आज सेरीकल्चर के निदेशक, कल कलेक्टर, फिर सीएम के सलाहकार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में काम करते हैं.
यह एक संतुष्टिदायक बात है. आईएएस होने के नाते हमारा निर्णय अंतिम नहीं है. कैबिनेट सचिवालय, सरकार, आरबीआई के गवर्नर के रूप में, मुझे निर्णय लेना है. यहां लिए गए फैसले का असर देश की जनता पर पड़ेगा. यह जिम्मेदार और चुनौतीपूर्ण लगता है. लेकिन हर काम का अपना आकर्षण और चुनौतियां होती हैं.
प्रश्न: आईएएस अधिकारियों ने पहले कॉर्पोरेट कंपनियों और राजनेताओं के साथ संबंधों में एक रेखा खींचने की आवश्यकता का हवाला दिया है. लेकिन अगर आप अभी देखें तो उस रेखा को पूरी तरह से मिटाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है! समझौता, जो मेरा है वह तुम्हारा है कि सोच बढ़ गई है, इस पर आप क्या कहते हैं?
उत्तर: जनहित की अवधारणा के चारों ओर एक रेखा खींचना महत्वपूर्ण है. यह व्यक्तिगत भी है. कुछ लोग सोचते हैं कि वे क्या नहीं खाते, छूते नहीं, ऑफिस, घर... यही प्रकार है. वे दूसरे प्रकार के हैं, जिनके पास मैं विनम्रता के लिए जाता हूं, लेकिन प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं कि जाना ग़लत है. इसलिए रेखा कहां खींचनी है यह व्यक्तिगत मामला है. किसी की स्थिति के अनुरूप गरिमा बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
मैंने यह भी सुना है कि आईएएस अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है. लेकिन आईएएस को किसी भी परिस्थिति में जनहित के विपरीत मामलों पर समझौता नहीं करना चाहिए. यदि झाड़ू में कोई चीज चिपक जाए, तो आप उसे तोड़ सकते हैं, लेकि पूरा बंडल नहीं तोड़ा जाता है! अगर सब लोग एक साथ हों तो कुछ नहीं किया जा सकता.'