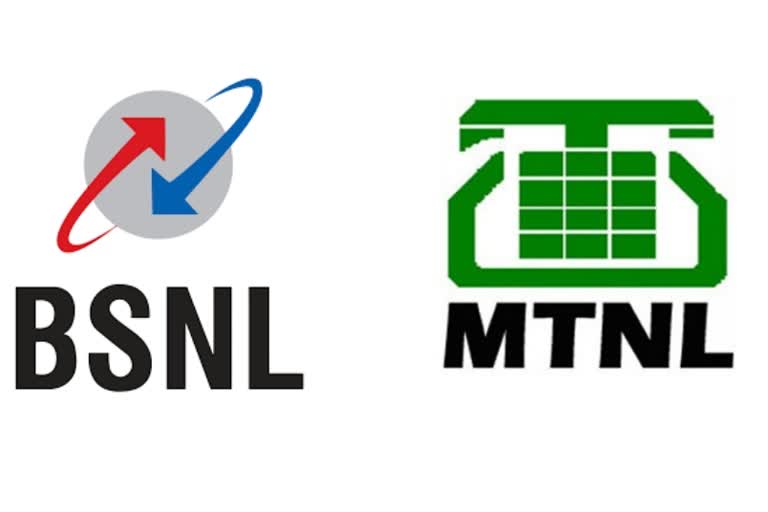नई दिल्ली : देश की बीमार दूरसंचार कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल का भविष्य ज्यादा सुनहरा नहीं दिख रहा है. मोदी सरकार द्वारा इन दोनों कंपनियों के विलय करने का फैसला शायद थोड़ी देर से आया है. पर, यह कदम भी इन कंपनियों को वापस पटरी पर लाने में नाकाफी साबित होगा.
जानकारों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से बाजार में बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए मुकाबला कड़ा ही रहेगा. केवल परिचालन के खर्चे पूरे हो सकेंगे. उनका कहना है कि सरकार को समय रहते ही पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत थी. लेकिन अब इस कदम से इन सरकारी कंपनियों के कायाकल्प होने की उम्मीद करना नाकाफी है. दोनों ही कंपनियां परिचालन के मामले में बड़े घाटों से घिरी हैं. कंपनियों के विलय और वीआरएस योजना से परिचालन के खर्चों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा, पर ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
बीएसएनएल और एमटीएनएल, जो एक जमाने में नवरत्न कंपनियों में शामिल थीं, 90 हजार करोड़ के नुकसान के साथ बीमार कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, बीएसएनएल का निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे कि रिलायंस, एयरटेल आदि से मुकाबला ना कर पाना. करीब 17 लाख कर्मचारियों के साथ बीएसएनएल इस दौड़ में पिछड़ती चली गई.
जानकारों की मानें तो बीएसएनएल और एमटीएनएल के पतन के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है इन कंपनियों के कर्मचारियों की मानसिकता, जो दशकों पुराने सिस्टम के हिसाब से चली आ रही थी. कंपनियां कर्मचारियों को मौजूदा जरूरतों के हिसाब से बदलने में नाकामयाब रहीं, और यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण रहा. इसके अलावा कुछ इलाकों को छोड़कर 4G की गैरमौजूदगी, कर्मचारियों के बड़े खर्चे और कम दाम बीएसएनएल के पतन के कारण बने.
2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद से सरकारी कंपनियों की कमाई में लगातार गिरावट आती गई. रिलायंस जियो ने अपने दामों से सारे दूरसंचार बिजनेस को हिला दिया. जियो के 4G के आने के बाद से देश में डाटा की खपत में तेजी से इजाफा हुआ है. इस बढ़त का फायदा इन सरकारी कंपनियों को नहीं मिल सका और इनकी कमाई लगातार गिरती गई. अब मैदान में केवल तीन निजी कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो बचीं हैं.
सरकारी दूर संचार कंपनियों को मौजूदा समय में दोबारा खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के साथ-साथ, 15,000 करोड़ के बांड लाने की भी तैयारी की है. सरकार वीआरएस भी ला रही है. 36 हजार करोड़ मूल्य की संपत्तियां भी बेचेंगी.
पढ़ें-BSNL और MTNL को पुनर्जीवित करने की जरुरत : शरद कोहली
एक नजरिये से देखें तो इन दोनों कंपनियों का विलय सही फैसला है. क्योंकि दोनो ही कंपनियां दो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं. एक ऐसे समय में जब सभी निजी कंपनियों की देशभर में मौजूदगी है, इन दोनों कंपनियों के विलय का फैसला सही लगता है. इस विलय से निजी कंपनियों को कुछ हद तक मुकाबला भी दिया जा सकता है. पहले से ही कर्जों में चल रही निजी कंपनियां अब अपने विस्तार पर तेजी नहीं दिखा रही हैं. ऐसे में एक मजबूत पीएसयू होने से दूरसंचार सेवाओं के दामों पर काबू पाने और देश के अन्य पिछड़े इलाकों में सेवाओं को पहुंचाने में मदद मिलेगी.
बीएसएनएल की मौजूदगी देश के लिए सामरिक लिहाज से भी जरूरी है. यह कंपनी देश के संवेदनशील संगठनों को जोड़ने का काम भी करती हैं. इसलिए यह और जरूरी हो जाती है. जब राष्ट्र सुरक्षा की बात हो, तो दूरसंचार बहुत जरूरी हो जाता है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी यह बात कही कि राष्ट्रीय आपदाओं के समय बीएसएनएल ने ही सबसे आगे आकर मुफ्त दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराई हैं.
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति
एक ऐसे समय में जब दुनिया भर में सूचना क्रांति का दौर चल रहा है, यह जरूरी है कि देश में सरकारी दूरसंचार कंपनी की मौजूदगी बनी रहे. 2018 में शुरू की गई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), में दूरसंचार मंत्रालय ने डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े मुख्य पहलुओं को चिह्नहित किया गया है. इनमें ब्रॉडबैंड की पहुंच, बेहतर रेडियो स्पेक्ट्रम, राष्ट्रीय दूरसंचार ढांचे की सुरक्षा आदि शामिल हैं. इन मुद्दों को साधने के लिए इस नीति में 'कन्नेक्ट इंडिया', 'प्रोपेल इंडिया' और 'सिक्योर इंडिया' जैसे एक्शन प्लान के बारे में कहा गया है.
कनेक्ट इंडिया के तहत ब्रॉडबैंड के इस्तेमाल से सामाजिक और आर्थिक विकास को हासिल किया जाए, प्रोपेल इंडिया से नई डिजिटल तकनीकों का विकास किया जाए और सिक्योर इंडिया के जरिये देश में डिजिटल संचार सेवाओं की सुरक्षा पर काम किया जाए.
भारत ने सरकारी दूरसंचार कंपनियों की मदद से इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2022 तक का समय रखा है.
वहीं हमारा पड़ोसी चीन इस क्षेत्र में काफी तरक्की कर चुका है. डिजिटल अर्थव्यवस्था में कामयाबी के साथ-साथ चीनी दूरसंचार कंपनियां देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद कर रही हैं.
हांलाकि ज्यादातर देशों में सरकारों ने दूरसंचार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी छोड़कर निजी कंपनियों को आने दिया है. लेकिन इस मामले में चीन एक अपवाद है. चीन ने पिछले साल ही 4G उपभोक्ताओं में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था.
इसमें सरकारी दूरसंचार कंपनियां: चाइना मोबाइल, चाइना टेलिकॉम और चाइना यूनिकॉम की हिस्सेदारी 65%, 18% और 17% रही. इस कराण से दुनियाभर के 4G उपभोक्ताओं में से 40 फीसदी चीन में हैं.
अगर भारत की बात करें तो, सरकारी निजी कंपनियों का बाजार शेयर, वायरलेस सब्स्क्राइबर में महज 10 फीसदी है और वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्स्क्राइबर बेस में केवल 3 फीसदी है. ट्राई के आंकड़ों की माने तो, 2019 तक बीएसएनएल का बाजार शेयर 9.8% था, जिसे एमटीएनएल के साथ मिला दें तो ये आंकड़ा 10.28% तक चला जाता है. इससे साफ है कि दूरसंचार क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों का प्रभुत्व स्थापित है.
इन कंपनियों को दोबारा खड़ा करने की अपनी योजना को लेकर सरकार अतिउत्साहित लग रही है. उसका मानना है कि 4G स्पेक्ट्रम के आने से बाजार में मुकाबला कड़ा हो जायेगा.
लेकिन मूल मसला है कि क्या बीएसएनएल बाजार के कड़े मुकाबले के लिए हर तरह से तैयार है? केवल 4G स्पेकट्रम से ही उपभोक्ता की गारंटी नहीं हो सकती है. ग्राहकों को प्रोडक्ट के साथ साथ सेवाओं की भी दरकार होती है. ग्राहकों से सीधे संबंध के मामलों में सरकारी कंपनियां काफी पिछड़ती हैं. ये इसलिए क्योंकि ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा सेवाओं की जरूरत होती है. इन दोनों ही सरकारी कंपनियों का कस्टमर सर्विस एक बड़ा कारण है कि लोग अन्य निजी कंपनियों की तरफ रुख करते हैं.
यह जरूरी है कि सरकार इन सरकारी दूरसंचार कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक सुदृढ़ योजना लेकर आए. किसी भी कंपनी को सही तरह से काम करने के लिए स्वायत्ता की जरूरत होती है. हांलाकि बहुत लंबे समय से सरकारी कंपनियों को सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी संपत्ति की तरह देखा जाता रहा है. इन्हीं कारणों से इन कंपनियों ने लगातार पुरानी हो चुकी तकनीकों में निवेश किया है. इन कारणों के चलते इन कंपनियों में लगातार गिरावट आती गई है.
कंपनियों को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ इन्हें चलाने के तरीकों में बदलाव लाना भी बेहद जरूरी है. इन कंपनियों के काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाने के लिए काफी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे. अगर इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो, आर्थिक मंदी के इस दौर में इन कंपनियों को दोबारा खड़ा करने की ये योजना और परेशानी का सबब बन सकती है. और अगर इस बार ये कंपनियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी, तो ये इन दोनों कंपनियों के लिए आखिरी दरवाजा साबित होगा.
(लेखक - नीरज कुमार)